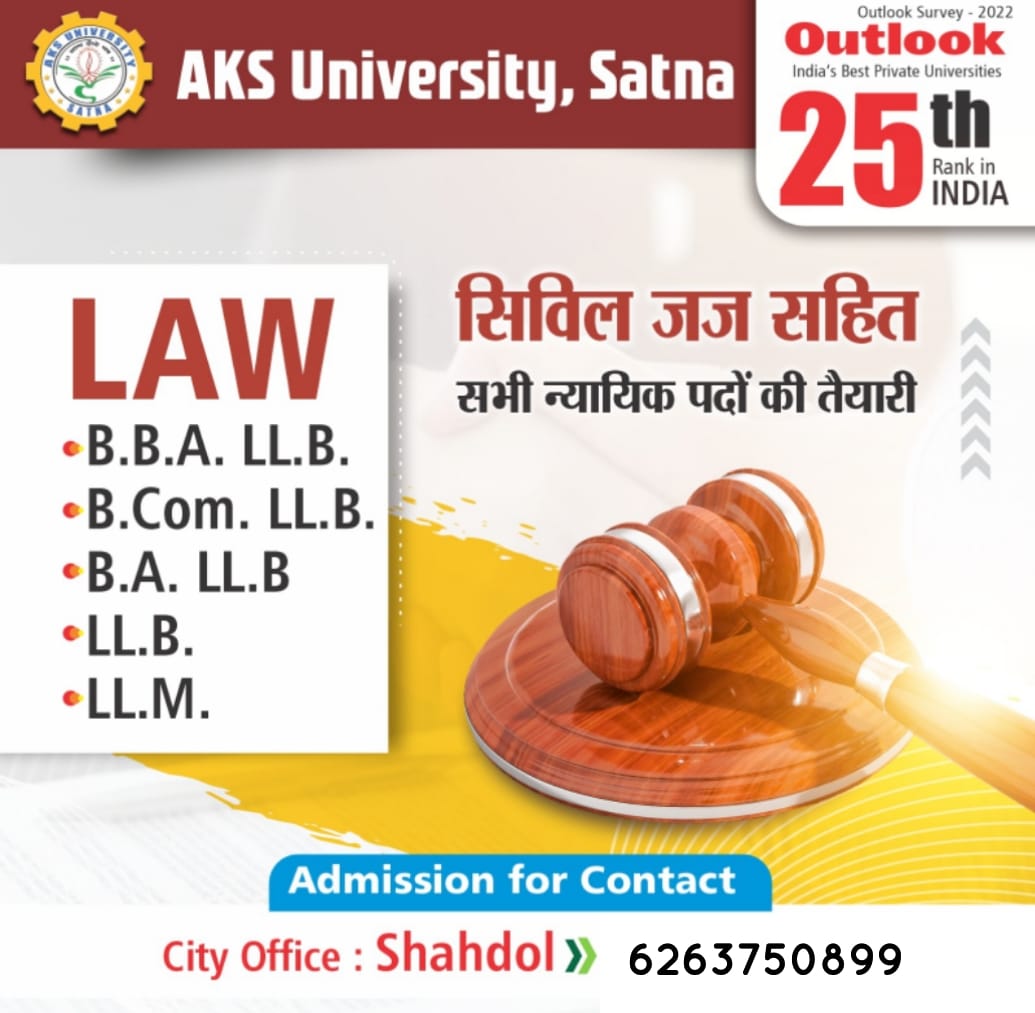चुनाव तारीखों की एलान होते ही आचार संहिता लागू, आखिर है क्या कोड ऑफ कंडक्ट, समझें सबकुछ

चुनाव तारीखों की एलान होते ही आचार संहिता लागू, आखिर है क्या कोड ऑफ कंडक्ट, समझें सबकुछ
आचार संहिता आखिर होती क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, क्यों लगाई जाती है, कब तक ये प्रभावशाली रहती है और इस दौरान क्या-क्या काम नहीं किए जा सकते। यदि ये सवाल आपके मन में भी हैं, तो खबर आपके लिए है।
मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में चुनावों की तारीख का एलान होते ही आचार संहिता (Code of Conduct) भी लागू हो गई। आचार संहिता आखिर होती क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, क्यों लगाई जाती है, कब तक ये प्रभावशाली रहती है और इस दौरान क्या-क्या काम नहीं किए जा सकते। यदि ये सवाल आपके मन में भी हैं, तो खबर आपके लिए है।
क्या होती है आचार संहिता
सबसे पहले समझते हैं कि आचार संहिता होती है, इसकी परिभाषा क्या है। आसान शब्दों में कहें तो आचार संहिता एक नियमावली है, जिसके तहत चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से करने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम-शर्तें तय करता है। या ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। इसकी परिभाषा की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के आयोजन हेतु अपने सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन में केन्द्र तथा राज्यों में सत्तारूढ़ दल (दलों) और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अधिकारी तंत्र का दुरूपयोग न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण यथा प्रतिरूपण, रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जा सके। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं।
आचार संहिता की शुरुआत कब से हुई
बता दें कि आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों की सर्वसहमति से लागू व्यवस्था है, ये कानून द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी, जिसमें बताया गया कि उम्मीदवार क्या कर सकता है और क्या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से आचार संहिता की व्यवस्था लागू हुई। तब से अब तक नियमित इसका पालन हो रहा है। हालांकि समय-समय पर इसके दिशा-निर्देशों में बदलाव होता रहा है।
आचार संहिता कब से कब तक प्रभावशाली रहती है
चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब चुनाव प्रोग्राम की तारीखें घोषित करता है, उसी के साथ ही आचार संहिता भी प्रभावशाली हो जाती है। यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक प्रवृत्त रहती है। या यूं कहें कि रिजल्ट आने तक ये प्रभाव में रहती है। चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दल, उम्मीदवार, सरकार और प्रशासन समेत चुनाव से जुड़े सभी लोगों पर इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है।
आचार संहिता में किन कामों पर होती है पाबंदी
इलेक्शन कमीशन की नियमावली के मुताबिक आचार संहिता लगने के बाद कई तहर के कामों पर रोक लगा दी जाती है। ये ऐसे काम होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। इस दौरान सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती। भूमिपूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकते। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज आदि का उपयोग वर्जित होगा। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है।
आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या होता है
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। नियमों के पालन में चुनाव आयोग राज्यों में सत्तारूढ़ दल और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण यथा प्रतिरूपण, रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जा सके। उल्लंघन के मामले मे उचित उपाय किए जाते हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, अथवा उल्लघंन करते पाया जाता है, तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है। दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है
प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की गणना शुरू होगी
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी के चुनावी खर्च पर सीमा तय कर रखी है। 2022 में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए राज्यों के आधार पर 54 से 70 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 70 से 95 लाख रुपये तय किया था। विधानसभा चुनावों में खर्च की सीमा को 20 से 28 लाख रुपये (राज्यों के आधार पर) से बढ़ाकर 28 से 40 लाख रुपये तय किया गया था। इसके लिए वर्ष 2020 में चुनाव खर्च की सीमा का अध्ययन करने के लिए चुनाव आयोग ने समिति का गठन किया था। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में 10% की वृद्धि के अलावा उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा में अंतिम बड़ा संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था। समिति ने पाया कि वर्ष 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है।
चुनावी खर्च में क्या-क्या होता है शामिल
चुनावी खर्च वह राशि है जो एक उम्मीदवार चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च करता है। इसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सभी व्यय का अलग और सही खाता रखना होता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों में उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है। यदि उम्मीदवार ने गलत विवरण प्रस्तुत किया तो अधिनियम की धारा 10 के तहत चुनाव आयोग उसे तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

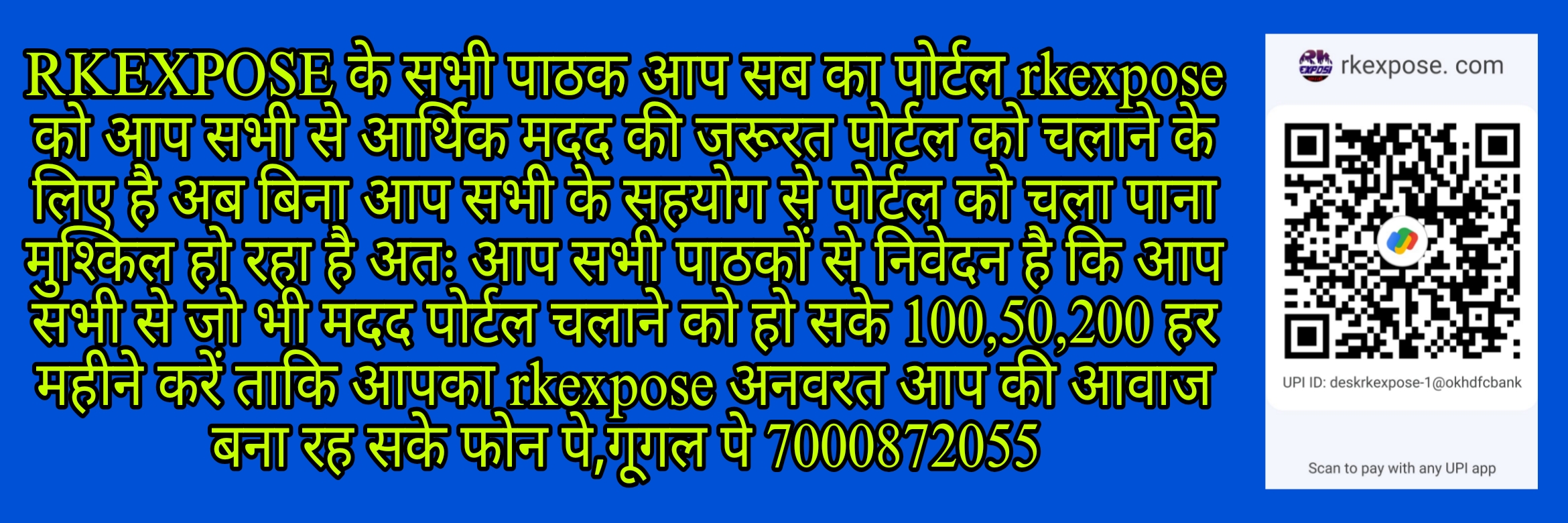




 rn
rn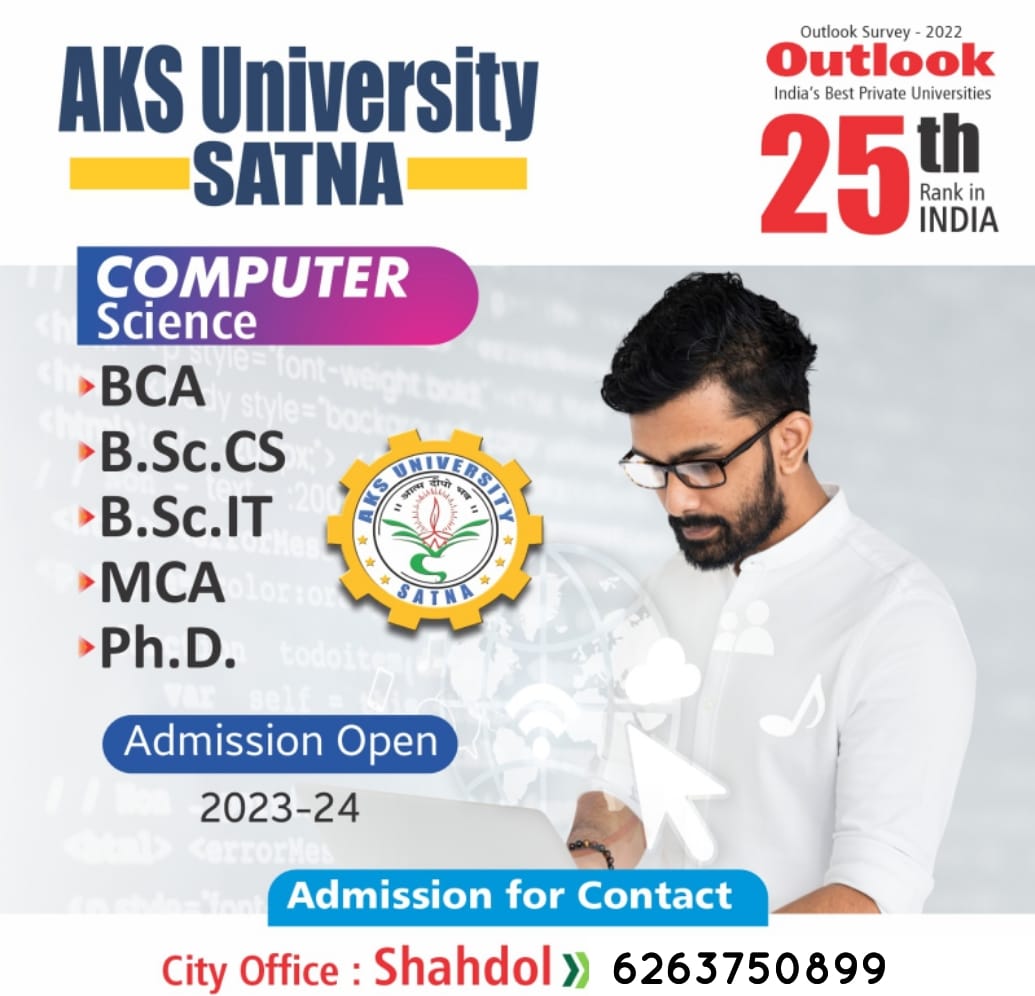 rn
rn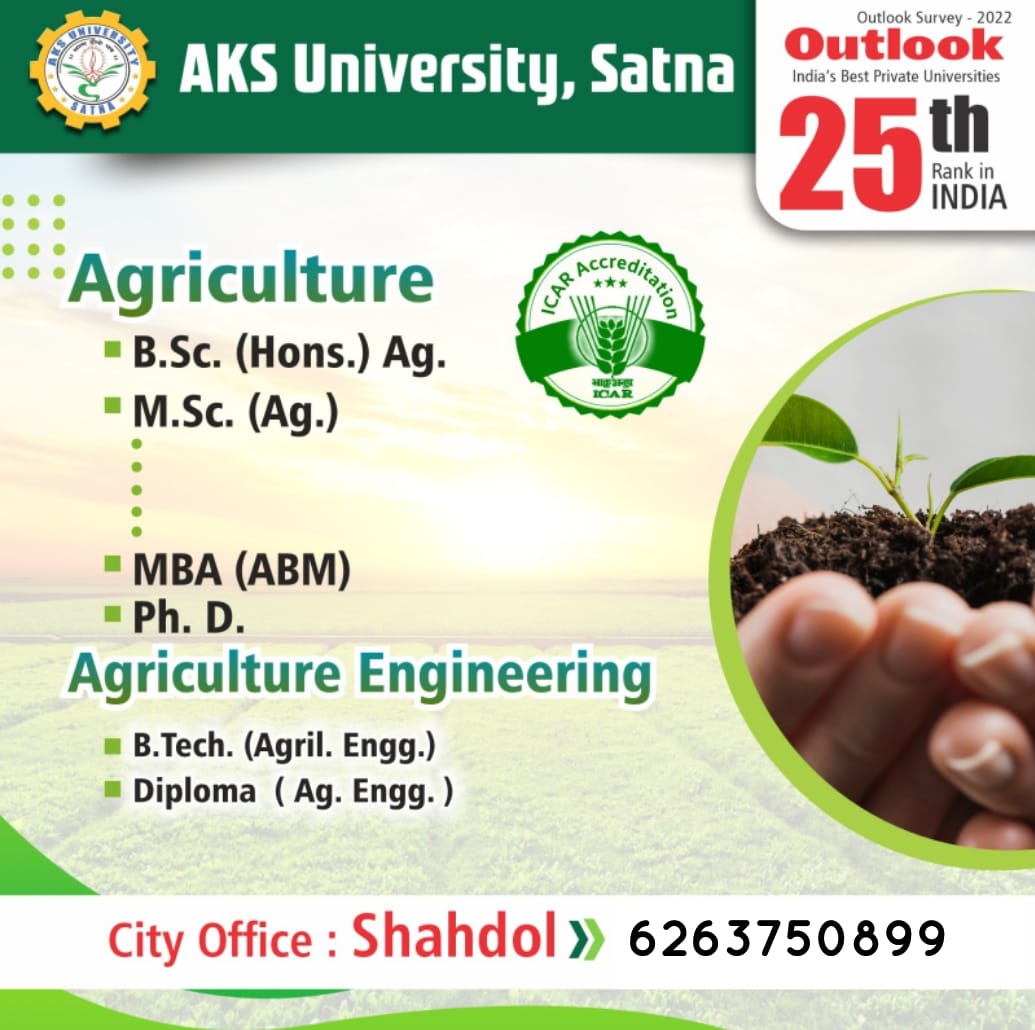 rn
rn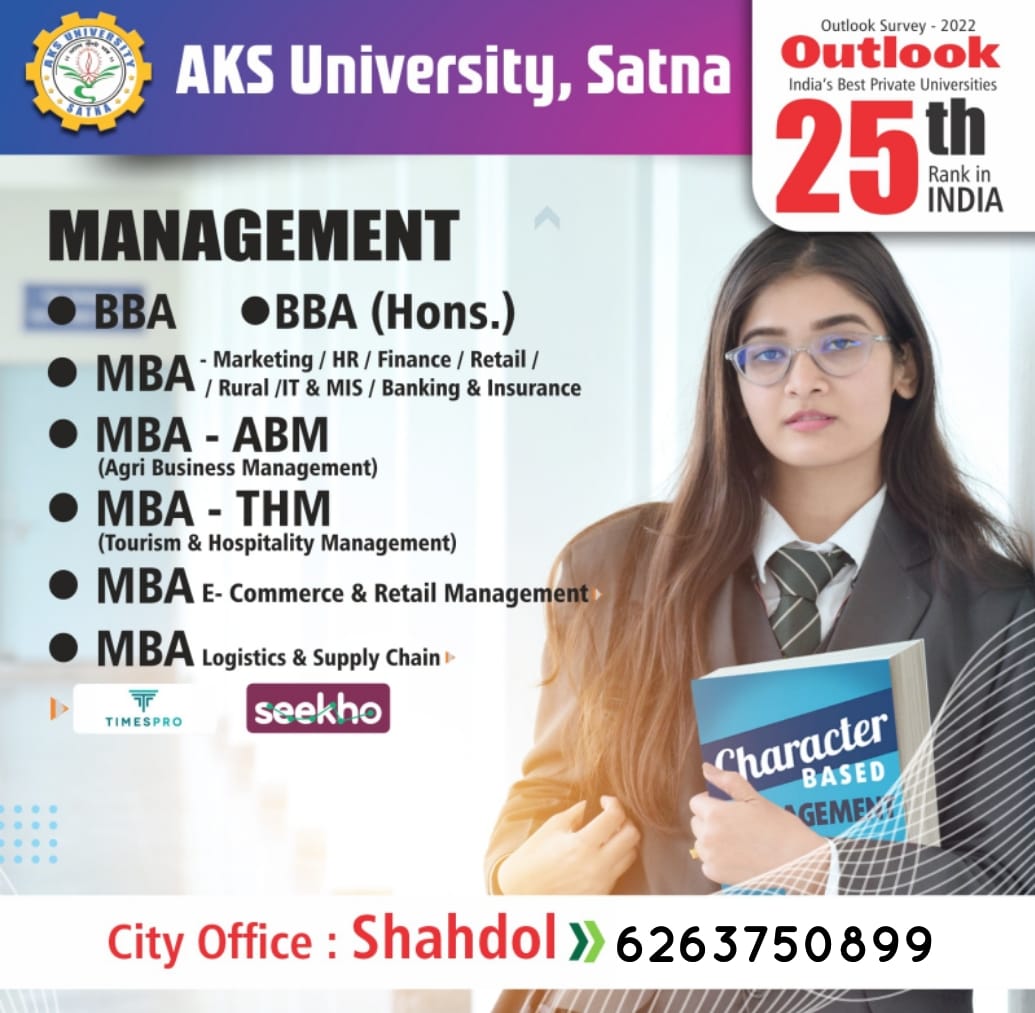 rn
rn rn
rn